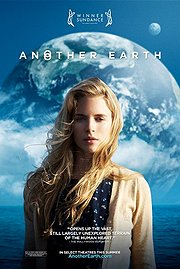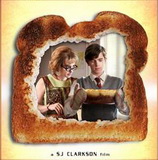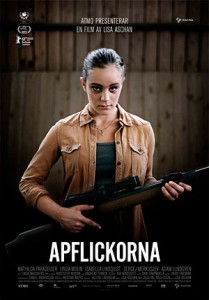फ़िल्म महोत्सवों में सदा विचारणीय आदिम प्रश्न यह है कि आखिर पांच समांतर परदों पर रोज़ दिन में पांच की रफ़्तार से चलती दो सौ से ज़्यादा फ़िल्मों में ’कौनसी फ़िल्म देखनी है’ यह तय करने का फ़ॉर्म्यूला आख़िर क्या हो? अनदेखी फ़िल्मों के बारे में देखने और चुनाव करने से पहले अधिक जानकारी जुटाना एक समझदारी भरा उपाय लगता है लेकिन व्यावहारिकता में देखो तो इसमें काफ़ी पेंच हैं. जैसे आमतौर पर अमेरिकी और यूरोपीय मुख्यधारा से इतर सिनेमा के बारे में जानकारियाँ हम तक पहली दुनिया के चश्मे से छनकर आती हैं. इन जानकारियों पर अति-निर्भरता नज़रिया सीमित कर सकती है. फ़ेस्टिवल कैटेलॉग पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, कई बार तो यही दस्तावेज़ सबसे भ्रामक साबित होता है. इन्हें तैयार करने वाले बहुधा ऐसे प्रशिक्षु सिनेमा विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने खुद भी इनमें से कम ही फ़िल्में देखी हैं.
बड़े नामों या निर्देशकों के पीछे अपना पैसा लगाने वाले हमेशा उस खूबसूरत सिनेमा अनुभव को खो बैठते हैं जिसकी सुंदरता अभी वृहत्तर सिने-समाज द्वारा रेखांकित की जानी बाक़ी है. और फिर प्रतिष्ठित सिनेमा महोत्सव में, जहाँ सिनेमा का स्तर इस क़दर ऊँचा हो कि हर देखी फ़िल्म के साथ समांतर चलती और हाथ से छूटने वाली फ़िल्मों के लिए अफ़सोस गहराता ही चला जाए, किसी फ़िल्म का ’प्लॉट’ भर जान लेना आख़िर कहाँ पहुँचाएगा?
सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण यह कि एक अनजाने से देश से आई किसी नई फ़िल्म को देखने से जुड़ा वो अनछुआ अहसास इन तमाम जानकारियों की भीड़ में कुचल जाता है. हमारे नज़रिए का कोरापन पहले ही नष्ट हो चुका होता है और सिनेमा अपना इत्र खो देता है. सूचना विस्फोट के इस अराजक समय में बिना किसी पूर्व निर्मित कठोर छवि के एक नई, कोरी फ़िल्म को देखने का विकल्प तो जैसे हमसे छीन ही लिया गया है.
हमारे दोस्त वरुण ग्रोवर इस मान्य विचार को चुनौती देने का प्रण करते हैं. वो अपनी बनते किसी फ़िल्म के बारे में कोई पूर्व जानकारी हासिल नहीं करते और उनके synopsis तो भूलकर भी नहीं पढ़ते. कुछ भरोसेमंद दोस्तों की सलाह पर हम किसी अनदेखी फ़िल्म के लिए थिएटर में घुस जाते हैं. और तभी हाल में अंधेरा होने से ठीक पहले परदे के सामने एक कमउमर लड़का आता है और पहले अपने सिनेमा अध्ययन करवाने वाले संस्थान का नाम ऊंचे स्वर में बताकर बतौर परिचय फ़िल्म की कहानी सुनाने लगता है. मैं वरुण की ओर देखता हूँ. वरुण अपने कानों में उंगलियाँ दिए बैठे हैं और माइक पर आती उसकी बुलन्द आवाज़ को अनसुना करने की भरसक, लेकिन असफ़ल कोशिश कर रहे हैं. मेरे सामने फिर एक बार यह साबित होता है कि इस सूचना विस्फोट के युग में जहाँ अनचाही सूचना का अथाह समन्दर सामने हिलोरें मारता है, हमारे भविष्यों में सिर्फ़ डूबना ही बदा है.
 The Turin Horse
The Turin Horse
Bela Tarr, Hungary, 2011.
भागते हुए सिनेमा हाल के गलियारों में पहुँचे और हम सीधे धकेल दिए जाते हैं बेला टार के विज़ुअल मास्टरपीस ’द तुरिन हॉर्स’ के सामने. सिर्फ़ विज़ुअल, क्योंकि परदे पर आवाज़ तो है लेकिन सबटाइटल्स गायब हैं. लेकिन बिना शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ जाने भी यह अनुभव विस्मयकारी है. एक तक़रीबन घटना विरल कथा में परदा श्वेत-श्याम दृश्य गढ़ रहा है. मैं देखने लगता हूँ. अन्दर तक भर जाता हूँ, साँस फूलने लगती है, लेकिन दृश्य में ’कट’ नहीं होता. धीरे-धीरे इन फ्रेम दर फ्रेम चलते अनन्त के साधक, सघन दृश्यों के ज़रिए वह सारा वातावरण और उसकी सारी ऊब, थकान मेरे भीतर भरती जाती है. मैंने अपने सम्पूर्ण जीवन में सिनेमा के उस विशाल परदे पर ऐसा विस्मयकारी कुछ होता कम ही देखा है.
लेकिन ठीक वहीं, हमें अभिभूत अवस्था में छोड़ फ़िल्म दोबारा न शुरु होने के लिए रोक दी जाती है. वादा किया जाता है रात का, लेकिन रात आती है उसी फ़िल्म के किसी घटिया डीवीडी प्रिंट के साथ. मैं पहले पन्द्रह मिनट की फ़िल्म देखकर उठ जाता हूँ. वह सुबह का उजला अनुभव अब भी मेरे पास है, मैं उसे यूं मैला नहीं होने दे सकता.
The Salesman
Sebastien Pilote, Canada, 2011.
यह हमारे वक़्तों का सिनेमा है. एक कस्बा है और उसके केन्द्र में उसकी तमाम अर्थव्यवस्था का सूत्र संचालक एक संयंत्र है. एक संयंत्र जो मंदी की ताज़ा मार में घायल है और अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है. यह उस संयंत्र की तालेबन्दी के बाद के कुछ निरुद्देश्य असंगत दिनों की कथा है. लेकिन यहाँ एक पेंच है. यहाँ कथा जिस व्यक्ति के द्वारा कही जाती है वह एक बुढ़ाता कार सेल्समैन है जिन्हें बीते खुशहाल सालों में अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होने के कई तमगे मिले हैं. लेकिन आज कस्बे में मरघट सा सन्नाटा है और संयंत्र बंद होने के बाद अब उससे जुड़ी तमाम उम्मीदें भी धीरे-धीरे कर दम तोड़ रही हैं. संकट यह है कि सेल्समैन को आज भी अपना काम करना है. सच-झूठ कैसे भी हो, उस शोरूम में खड़ी नई-नवेली कार का सौदा पटाना है.
मुझे सीन पेन की क्लासिक फ़िल्म ’दि असैसिनेशन ऑफ़ रिचर्ड निक्सन’ याद आती है. यह एक ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में बयान है जिसमें इंसान का दोगलापन उसका तमगा और उसकी ईमानदारी उसके करियर के लिए बाधा समान है. यहाँ इंसान को आगे बढ़ने के लिए पहले अपने भीतर की इंसानियत को मारना पड़ता है. व्यवस्था बदली नहीं है, बस हुआ यह है कि इस वैश्विक महामंदी ने इस व्यवस्था के दोगले मुखौटे को उतार दिया है. अगर आप सुनने की चाहत रखते हों तो इस फ़िल्म के मंदीमय बर्फ़ीले सन्नाटे में भविष्य में होनेवाले ’ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट’ की आहटें सुन सकते हैं.
 Michael
Michael
Markus Schleinzer, Austria, 2011.
पहले ही बता दिया गया था कि यह फ़िल्म इस समारोह की बहुप्रतिक्षित ’डार्क हॉर्स’ है. निर्देशक मार्कस तोप जर्मन निर्देशक माइकल हेनेके के लम्बे समय तक कास्टिंग डाइरेक्टर रहे हैं और ’दि व्हाइट रिबन’ के लिए तमाम बच्चों की चमत्कारिक लगती कास्टिंग उन्हीं का करिश्मा थी. ’माइकल’ का प्लॉट विध्वंसक है. यह फ़िल्म घर के तहखाने में कैद किए एक बच्चे और उसके यौन शोषक नियंता की दैनंदिन जीवनी को किसी रिसर्च जर्नल की तरह निरपेक्ष भाव से दर्ज करती अंत तक चली जाती है.
’माइकल’ का चमत्कार उसकी निर्लिप्त भाव कहन में है. फ़िल्म कहीं भी निर्णय नहीं देती. कहीं भी फ़ैसला सुनाने की मुद्रा में नहीं आती और यथार्थ को इस हद तक निचोड़ देती है कि परिस्थिति का ठंडापन भीतर भर जाता है. असहज करती है, लेकिन किसी ग्राफ़िकल दृश्य से नहीं, बल्कि अपने कथानक के ठंडेपन से. घुटन महसूस करता हूँ, मेरा अचानक बीच में खड़े होकर चिल्लाने का मन करता है. कहीं यह हेनेके की शैली का ही विस्तार है. ’माइकल’ एक सामान्य आदमी है. नौकरीपेशा, छुट्टियों में दोस्तों के साथ हिल-स्टेशन घूमने का शौकीन, त्योंहार मनाने वाला. दरअसल उसका ’सामान्य’ होना ही सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हम ऐसे अपराधियों की कल्पना किसी विक्षिप्त मनुष्य के रूप में करने के आदी हो गए हैं. निर्देशक मार्कस उसे यह सामान्य चेहरा देकर जैसे हमारे बीच खड़ा कर देते हैं. सच है, यह यथार्थ है. और यह भयभीत करता है.
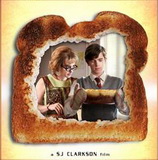 Toast
Toast
J S Clarkson, UK, 2011.
ब्रिटिश फ़िल्म ’टोस्ट’ की शुरुआत मुझे रादुँगा प्रकाशन, मास्को से आई हमारे घर के बच्चों की खानदानी किताब ’पापा जब बच्चे थे’ की किसी कहानी की याद दिलाती है. लेकिन अंत में नीति कथा बन जाती उन स्वभाव से उद्दंड रूसी बाल-कथाओं से उलट ’टोस्ट’ सदा उस बच्चे के नज़रिए से कही गई कथा ही बनी रहती है. इसे देखते हुए लगातार विक्रमादित्य मोटवाने की ’उड़ान’ याद आती है और मैंने इसे कुछ सोचकर ’फ़ीलगुड’ उड़ान का नाम दिया. कहानी में कायदा सिखाने वाले, बाहर से सख़्त, भीतर से नर्म पिता हैं. ममता की प्रतिमूर्ति साए सी माँ हैं, और हमारा कथानायक आठ-दस साल का नाइज़ेल है. और सबसे महत्वपूर्ण यह कि रोज़ नाइज़ेल के सामने घर का डब्बाबंद खाना है जिसे अधूरा छोड़ वह असली, लजीज़ पकवानों के ख्वाब देखा करता है.
आगे कहानी में माँ की मौत से लेकर सौतेली माँ तक के तमाम ट्विस्ट हैं. स्त्रियों का वही परम्परा से चला आया स्टीरियोटाइप चित्रण है जो खड़ूस सौतेली माँ की भूमिका में हेलेना कार्टर की अद्भुत अदाकारी की वजह से और उभरकर सामने आता है. ’टोस्ट’ कथा धारा के परम्परागत ढांचे को तोड़ती नहीं है. लेकिन उसे एक मुकम्मल कथा की तरह ज़रूर कहती है. हाँ, बचपन में नाइज़ेल के उस दोस्त का किरदार कमाल का है जो उसे हमेशा ज्ञान देता रहता है. सच कहूँ, यह भी एक स्टीरियोटाइप ही है लेकिन ऐसा जिसका सच्चाई से सीधा वास्ता है. मुझे अपने बचपन का साथी दीपू याद आता है जो मुझसे एक साल सीनियर हुआ करता था और मुझे हर आनेवाली क्लास के साथ अगली क्लास की अभेद्य चुनौतियों के बारे में बताया करता था. यहाँ भी उसका दोस्त वक़्त-बेवक़्त ’नॉर्मल फ़ैमिलीज़ आर टोटली ओवररेटेड’ जैसे वेद-वाक्य सुनाता चलता है. कथा का अंत फिर इसे ’उड़ान’ से कहीं गहरे जोड़ता जाता है.
 The Ides of March
The Ides of March
George Clooney, USA, 2011.
यह वो महत्वाकांक्षी हॉलीवुड थ्रिलर है जिसके लिए स्क्रीन के बाहर लम्बी लाइनें लगीं और संभवत: जिस फ़िल्म की गूंज आप आनेवाले ऑस्कर पुरस्कारों में सुनेंगे. सत्ता है, हत्या है, महत्वाकांक्षाएं हैं, फ़रेब है, ऊपर दिखती खूबसूरती है, बदनुमा अतीत है. लेकिन जॉर्ज क्लूनी निर्देशित ’द आइड्स ऑफ़ मार्च’ की जान फ़िल्म के नायक रेयान गॉसलिंग हैं. पता हो, यह लड़का पिछले साल ’ब्लू वेलेंटाइन’ जैसी घातक रूप से अच्छी फ़िल्म दे चुका है. जॉर्ज क्लूनी और मेरे पसन्दीदा फ़िलिप सिमोर हॉफ़मैन जैसे खेले-खाए अदाकारों के सामने इस तीस साल के लड़के की धमक सुनने लायक है. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के चुनाव के लिए मतदान के दौरान की इस कथा में हमारे समय के हालिया वर्तमान से निकले अनेक स्वर सुनाई देते हैं. किसी पर्फ़ेक्ट राजनैतिक थ्रिलर की तरह कथा आपको बांधे रखती है और जहाँ होना चाहिए वहाँ मोहभंग भी होता है, लेकिन परेशानी यही है कि फ़िल्म जहाँ बनती है ठीक वहीं ख़त्म हो जाती है.
इस बीच दोस्तों की चर्चाओं में लौट-लौटकर ’माइकल’ आती रही. एक दोस्त ने कहा कि वह अपराधी का मानवीकरण है. मुझे याद आया कि ’सत्या’ के बाद उसे भी स्थापित करते हुए आलोचकों ने यही कहा था कि यहाँ पहली बार एक ’डॉन’ का मानवीकरण होता है, उसके भी बीवी-बच्चे हैं. वो दोस्त की शादी की बरात में नाचता है. वो भी चाहता है कि उसकी बच्ची स्कूल में अंग्रेज़ी पोएम सीखे. तो क्या ’माइकल’ भी ’सत्या’ की तरह अपराधी का मानवीकरण करती है? यह भी एक नज़रिया है जिससे मैं असहमत हूँ. उसकी निर्पेक्षता मेरे भीतर और ज़्यादा सिहरन भर देती है. यह अहसास कि एक भयानक अपराधी भी कितने ही मामलों में ठीक हमारे जैसा है, उसके और हमारे बीच की दूरी एकदम कम कर देता है. और सच्चाई यह है कि इस दूरी के मिटने से ज़्यादा डरावना किसी भी ’सभ्य समाज’ के नागरिक के लिए कुछ और नहीं हो सकता.
 Tabloid
Tabloid
Errol Morris, USA, 2010.
यह संयोग ही था कि हम एरॉल मोरिस की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ’टैबलॉयड’ देखने घुसे. और यह फ़िल्म तुरंत इस साल देखे गए कुछ दुर्लभ वृत्तचित्रों की लम्बी होती लिस्ट में शामिल हो गई. बहुत की रोचक अंदाज़ और आर्ट डिज़ाइन के साथ बनाई गई इस फ़िल्म की असल तारीफ़ इस बात में छिपी है कि निर्देशक ने कैसे मामूली से दिखते एक ’अखबारी कांड’ में इस गैर-मामूली फ़िल्म को देखा और बनाया. कैसे किसी की व्यक्तिगत ज़िन्दगी को मौका आने पर पीत-पत्रकारिता सरेराह उछालती है और खुद ही न्यायाधीश बन फ़ैसले करती है. और ब्रिटेन के टैबलॉयड जर्नलिज़्म को समझने के लिए यह फ़िल्म दस्तावेज़ सरीख़ी है. इसके तीस साल पुराने घटनाचक्र में आप आज बन्द हुए ’न्यूज़ ऑफ़ द वर्ल्ड’ की तमाम कारिस्तानियाँ सुन सकते हैं.
17 Girls
Muriel Coulin and Delphine Coulin, France, 2011.
ये कुछ ऐसा था जैसे सत्रह लड़कियाँ आकर हमारे समाज से अपना शरीर, उस पर उनका अपना हक़ हमसे वापस मांगे. दोनों निर्देशक बहनों ने फ़िल्म से पहले आकर बताया था कि यह घटना भले ही कहीं और घटी और उन्होंने इसका ज़िक्र उड़ता हुआ अखबार के किसी पिछले पन्ने पर पढ़ा था, लेकिन कहानियाँ वे अपने घर, अपने कस्बे की ही सुनाती हैं. कैसे खुद उनके लड़कपन उन सीखों से भरे हुए थे जो लड़कियों को हमारे इन ’सभ्य’ समाजों में विरासत में मिलती हैं और कैसे वे नया जानने की, कुछ कर गुज़रने की बेचैनी से भरी थीं.
 मेरी राय में ’17 गर्ल्स’ के कथाकेन्द्र में मौजूद ’गर्भधारण’ सिर्फ़ एक कथायुक्ति भर है. इसकी जगह कोई और युक्ति भी होती, अगर इतनी ही कारगर तो भी यह कथा संभव थी. क्योंकि यह मातृत्व के बारे में नहीं है. न ही यह सेक्स लिबरेशन जैसे किसी विचार के बारे में है. दरअसल यह कथा सामूहिकता के बारे में है. उस युवता के बारे में है जो जब साथ होती है तो दुनिया बदलने की बातों वाले किस्से अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं. आकाश के सितारे कुछ और पास लगते हैं. हमउमर साथ खड़े होते हैं, बाहें फ़ैलाते हैं और एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट लेते हैं. बस, फिर किसी और पीढ़ी की, उनकी सीखों की, उनकी समझदारियों की ज़रूरत नहीं रहती. अजीब लगेगा, लेकिन इस फ़िल्म को देखते हुए मुझे भगतसिंह और उनके साथी याद आते हैं. उनकी तरुणाई और उनके अदम्य स्वप्न याद आते हैं. आज यह ’व्यक्तिगत ही राजनैतिक’ है वाला ज़माना है और इन लड़कियों की आँखों में भी मुझे वही सुनहले सपने दिखाई देते हैं.
मेरी राय में ’17 गर्ल्स’ के कथाकेन्द्र में मौजूद ’गर्भधारण’ सिर्फ़ एक कथायुक्ति भर है. इसकी जगह कोई और युक्ति भी होती, अगर इतनी ही कारगर तो भी यह कथा संभव थी. क्योंकि यह मातृत्व के बारे में नहीं है. न ही यह सेक्स लिबरेशन जैसे किसी विचार के बारे में है. दरअसल यह कथा सामूहिकता के बारे में है. उस युवता के बारे में है जो जब साथ होती है तो दुनिया बदलने की बातों वाले किस्से अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं. आकाश के सितारे कुछ और पास लगते हैं. हमउमर साथ खड़े होते हैं, बाहें फ़ैलाते हैं और एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट लेते हैं. बस, फिर किसी और पीढ़ी की, उनकी सीखों की, उनकी समझदारियों की ज़रूरत नहीं रहती. अजीब लगेगा, लेकिन इस फ़िल्म को देखते हुए मुझे भगतसिंह और उनके साथी याद आते हैं. उनकी तरुणाई और उनके अदम्य स्वप्न याद आते हैं. आज यह ’व्यक्तिगत ही राजनैतिक’ है वाला ज़माना है और इन लड़कियों की आँखों में भी मुझे वही सुनहले सपने दिखाई देते हैं.
दर्जन से ज़्यादा किशोरवय लड़कियों का सामुहिक गर्भधारण का यह फ़ैसला उनके घरवालों को, स्कूल को हिला देता है. उनके लिए इसे समझ पाना मुश्किल है. वाजिब है, उन्हें ’नैतिकता’ खतरे में दिखाई देती है. लेकिन उन लड़कियों के लिए यह मृत्यु ज्यों शान्ति से भरे उस कस्बे के ठंडे पानी में एक पत्थर मारने सरीख़ा है. यह उन तमाम परम्पराओं का अस्वीकार है जिन्हें हमारे स्कूलों में बड़े होते नागरिकों पर एक अलिखित ’नैतिक शिक्षा’ के नाम पर थोपा जाता है. एक पिता के झिड़ककर कहने पर कि “तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया बदल सकती हो?” उसकी बेटी जवाब में कहती है, “कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकती हैं.”
*****
साहित्यिक पत्रिका ’कथादेश’ के दिसम्बर अंक में प्रकाशित